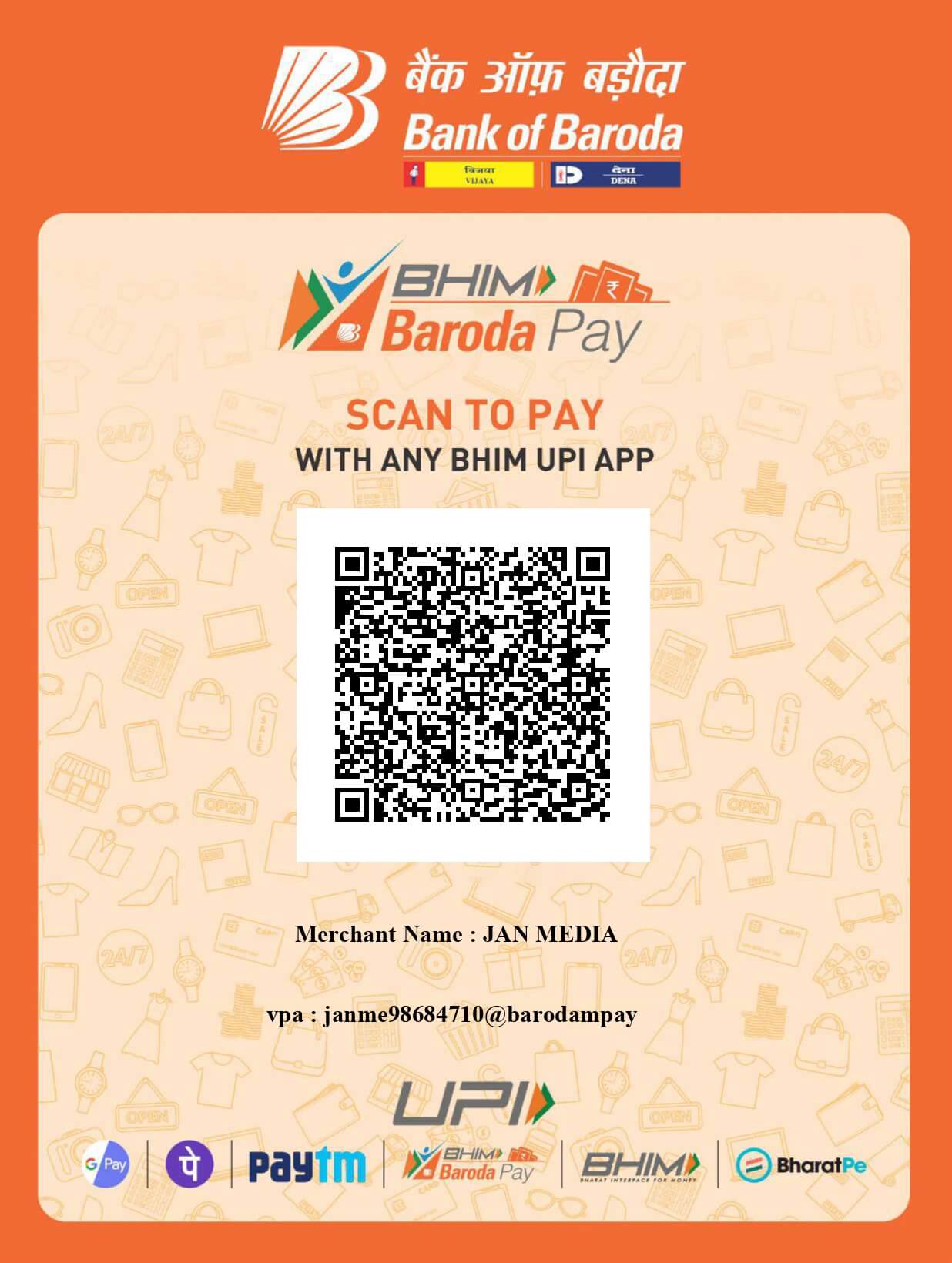सिनेमा हमारी दृष्टि को एक ऐसे संसार से बदल देती है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होता है। – आंद्रे बाज़ां
मैंने पच्चीस साल बाद गुरु दत्त की महत्त्वाकांक्षी फ़िल्म काग़ज़ के फूल देखी। यह फ़िल्म कैनेडी सेंटर के अमेरिकन फ़िल्म इंस्टीट्यूट के थियेटर मे आयोजित फ़िल्म उत्सव भारत-86 (वाशिंगटन डी.सी. 8 मई से 10 जून, 1986) के दौरान दिखायी गयी थी। मुझे यह फ़िल्म अत्यंत रोचक और मनोरंजक लगी और इसकी रोचकता इसकी उदास और चिंतनशील रुग्णता में निहित है। काग़ज़ के फूल व्यक्ति और फ़िल्म निर्देशक के तौर पर गुरुदत्त का स्वनिर्देशित सिनेमाई मृत्युलेख है। निकटस्थ स्तर पर यह निर्देशक-नायक (सुरेश) और गुरुदत्त का मृत्युलेख है। जिन्होंने इसके बाद कोई फ़िल्म निर्देशित नहीं की। अपने चरम स्तर पर यह 1964 में आत्महत्या द्वारा अपनी मृत्यु की अग्रिम सूचना है। काग़ज़ के फूल एक आत्मकथात्मक फ़िल्म है जिस पर एक झीना सा पर्दा पड़ा हुआ है। इसे गुरुदत्त की सर्वाधिक निजी फ़िल्म मानी जा सकती है। इसमें अपने जीवन, सिनेमा और विश्व के बारे में गहन अनुभूत दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। फ़िल्म बाॅक्स आॅफिस पर पूरी तरह नाकामयाब रही और एक भविष्यवाणी पूरी हुई। गुरुदत्त का विषाद की तरफ बढ़ना (जो प्यासा से स्पष्ट है) और जिसकी संभावना थी, वह काग़ज़ के फूल की व्यावसायिक मृत्यु ने सुनिश्चित कर दिया। यह सही है कि काग़ज़ के फूल के बाद भी उन्होंने कई कामयाब फ़िल्में बनायीं लेकिन जो अपरिहार्य घटित होना था, उससे पहले थोड़ा सांस लेने का समय उन्हें मिल गया था।
काग़ज़ के फूल गहरे रूप से एक दोषपूर्ण फ़िल्म है। उसका बाॅक्स आॅफिस पर नाकामयाब होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। एक केक अपने बिना पके हुए अवयवों से कुछ अधिक होता है। अंश से संपूर्ण सदैव महान होता है। काग़ज़ के फूल में बहुत ही जीवंत और रोचक अवयव हैं जिनका गुरुदत्त बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सके। उन्हें फ़िल्म में संतोषप्रद ढंग से एकीकृत नहीं कर सके। उन्होंने मधुर स्वाद की कल्पना की लेकिन जो मुझे आनंद देने में असफल रही। फिर भी, मेरी जीभ ने अस्पष्ट रूप से ही सही उस स्वाद को पहचान लिया था। हालांकि मोटे तौर पर इसकी गुणवत्ता औपचारिक ही हैं, इसके विश्लेषण को सुगम बनाने के लिए इसकी अंतर्वस्तु की रूपरेखा को संक्षेप में प्रस्तुत करना रोचक होगा। इसका कथानक निम्नानुसार हैः
फ़िल्म निर्देशक सुरेश (गुरुदत्त) अपनी पत्नी (वीणा) और बेटी (नाज़) से अलग रहता है। बहुत अधिक विद्वेष के बीच वह देवदास के एक नये संस्करण पर फ़िल्म बना रहा है। संयोग से उसकी मुलाकात शांति (वहीदा रहमान) से होती है जिसे सुरेश अपनी फ़िल्म में मुख्य भूमिका देता है जिसे जबर्दस्त कामयाबी मिलती है। निर्देशक और अभिनेत्री एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हालांकि परिस्थितियां उनके मिलन की अनुमति नहीं देती। अगली फ़िल्म असफल रहती है। अब सुरेश अपने परिवार, प्रेमिका, निर्माता और दर्शकों से विमुख हो जाता है और व्यावसायिक और निजी तौर पर उसका पतन होने लगता है। एक दिन उस स्टुडियो में जहां उसने कभी कामयाबी देखी थी, वह निर्देशक की कुर्सी पर गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ मरा हुआ मिलता है।
इस प्रकार काग़ज़ के फूल फ़िल्म-के भीतर-फ़िल्म विधा से संबंधित फ़िल्म है जो मानव परिस्थिति के विभिन्न पक्षों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के क्रम में यथार्थ और कथा के विभिन्न स्तरों की तुलना की सशक्त समृद्ध संभावनाएं प्रदान करती है। यह एक ऐसी विधा है जिसका बहुत कामयाब प्रयोग फ्रांस के ‘न्यू वेव’ के निर्देशक ज्यां-लक गोदार ने अपनी बहुत-सी उत्कृष्ट “प्रयोगधर्मी सिनेमा” फ़िल्मों जैसे La Mapris (कंटेप्ट), Pierrot Fou (Passion) इत्यादि में किया है। अपनी फ़िल्मों की अंतर्वस्तु को परिवर्धित करने के क्रम में अपनी चतुराई और साहित्यिक कार्यों, चित्रों, ऐतिहासिक घटनाओं, अन्य फ़िल्मों, उपभोक्ता उत्पादों इत्यादि की ओर संकेतों (यानी अप्रत्यक्ष संदर्भों) के लगभग विश्वकोशीय उपयोग के कारण ही काग़ज़ के फूल के लिए गोदार की फ़िल्में काफी प्रासंगिक हैं। बहुत कम हिंदुस्तानी फिल्में (श्याम बेनेगल की भूमिका ऐसी हैं जिनमें काग़ज़ के फूल की तरह संकेतों को उतने समृद्ध ढंग से लाभ उठाने की कोशिश की है। फ़िल्म में जो श्रेष्ठता निहित है वह इसके दृश्य और/या श्रव्य आख्यानों की लंबाई द्वारा प्रकट होने की बजाए इसके संकेतों में निहित है।
एक स्पष्ट संकेत फ़िल्म के शीर्षकः काग़ज़ के फूल में निहित है। काग़ज़ का फूल एक फरेब है, ऐसी वस्तु जो अपने में कुछ नहीं है। यह इसके वास्तविक नमूने की प्रतिलिपि (या प्रतिबिंब) है। काग़ज़ का फूल वास्तविकता का अमूर्तन (यानी अवधारणात्मक माॅडल) है। हालांकि काग़ज़ के फूल के निर्माण में सत्याभास की वास्तविक कोशिश होती है। काग़ज़ के फूल को धोखेे की तरह देखा जा सकता है क्योंकि इसके निर्माण में एक हद तक छल निहित होता है। इस प्रकार एक चेतावनी दी जाती है। फिर भी, फ़िल्म यथार्थवादी (वृत्तचित्र) आख्यान को अंगीकार करती है जो कि वास्तविक घटनाओं के साथ बहुत ज्यादा तादात्म्य स्थापित नहीं करती। यह यथार्थ की तरह है लेकिन स्वयं में यथार्थ नहीं है यानी इसका यथार्थवाद भ्रामक है। यहां गहन आधिभौतिक संदर्भ यह है कि हिंदू अवधारणा के अनुसार भौतिक दुनिया दरअसल माया है यानी एक मिथ्या वास्तविकता। इस रवैये की शून्यवादी परिणति आगे विचार करने के लिए बहुत स्पष्ट है। मैं इसे संकेत के रूप में छोड़ता हूँ। तथापि अपने निकटवर्ती अर्थ में, काग़ज़ के फूल की विशिष्टता उसमें जीवन की अनुपस्थिति है। काग़ज़ का फूल जीवन से रहित पुष्पित विन्यास है-एक मृत फूल। यह फ़िल्म मृत्यु के बारे में है। एक मृत्युलेख। दरअसल, जहां तक फ़िल्म एक प्रक्रिया है, हमंे मृत्यु को घटित होता और मृत्युलेख लिखे जाने की प्रक्रिया देखने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच यह स्पष्ट नहीं है कि यहां क्या यथार्थ है और कौन सा काग़ज का फूल है? फ़िल्म में निहित फ़िल्म (देवदास) में दुनिया चित्रित है? अपने आप में फ़िल्म? दोनों एक साथ? (आखिरकार फ़िल्म का शीर्षक बहुवचन में है)। किस “यथार्थ” पर यह आधारित है? क्या सब माया है? हम सभी जानते हैं कि कुछ साल बाद एक सचमुच की मौत घटित होती है। या की गई? ई. एम. फोस्टर ने लिखा है, “मृत्यु मनुष्य को नष्ट कर डालती है और मृत्यु का विचार उसे बचाता है”। लेखक-आलोचक Susan Sotang ने लिखा है कि “सभी फोटोग्राफ मृत्यु का स्मरण कराते हैं। तस्वीर खींचने का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति की नश्वरता में, असुरक्षा में और परिवर्तनीयता में सहभागी बनना।” फोटोग्राफी के आविष्कार ने यथार्थ के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है–“एक घटना के होने का अर्थ है, निश्चित रूप से उसकी तस्वीर ली जा सकती है” (सोंटेग)। गुरुदत्त ने स्वयं जीवन को अस्वीकार किया। उन्होंने दुनिया की वास्तविकता को भले ही अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन स्वयं अनश्वरता को खारिज नहीं कर सके। इसलिए वह यह विश्वास करते थे कि कोई चीज यदि माया से बचा सकती है तो वह तस्वीर में अंकित घटना है। काग़ज़ के फूल में भले ही जीवन न हो फिर भी, जिस चीज का दरअसल महत्त्व है वह है इसमें संरक्षित जीवन का विन्यास (विचार)। जो भी हो, शीर्षक में अस्तित्व के यथार्थ के बारे में गुरुदत्त के संशय का अनुकरण निहित है। इस संशय कीे सामाजिक-राजनीतिक परिणतियों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा।
काग़ज़ के फूल सिनेमास्कोप में बनी एक श्वेत-श्याम अद्वितीय हिंदुुस्तानी फ़िल्म है। आइए, इसके विषम आकार के फ्रेम पर थोड़ा ठहरते हुए और फिर इसके रंग (या, इसकी अनुपस्थिति) पर विचार करें।
सिनेमास्कोप फ्रेम का अनुपात 1ः1.35 होता है जबकि सामान्य फ्रेम का आकार 1ः1.33 होता है। काग़ज़ के फूल के लिए चैड़े फ्रेम के चयन का कारण संभवतः निम्नलिखित हैंः (і) फ़िल्म को महाकाव्यात्मकता (नायकत्व) प्रदान करना, (іі) देवदास के सामान्य फ्रेम को उससे बड़े आकार के काग़ज़ के फूल के फ्रेम में समाहित करना, (ііі) सुरेश की स्त्रियों के साथ संबंध में आने वाली मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कठिनाइयों की ओर इंगित करना (सर्गेइ आइसंेस्टिन ने क्षैतिज- सिनेमास्कोप का अनिवार्य गुण- और नारीत्व के बीच संबंधों के महत्त्व की ओर ध्यान खींचा है), और (іअ) मृत्यु के समय मानव शरीर की स्थिति को क्षैतिज से जोड़ना।
जब सेंचुरी-फाॅक्स ने पहली बार (दि रोब, 1953) सिनेमास्कोप को प्रस्तुत किया तो यह दावा किया गया कि “लोग चीजों को उस रूप में देखेंगे जिस रूप में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा”। दि रोब फ़िल्म के सिनेमाटोग्राफर लियोन शिमाॅय ने कहा था कि सिनेमास्कोप अगतिशील कैमरे के द्वारा लोगों को गति में (विशेष रूप से भीड़ को) देखने की अनुमति देता है। इस प्रकार, इस उपकरण के द्वारा हम दुनिया की “ईश्वरीय दृष्टि” का अनुभव प्राप्त करते हैं। गुरुदत्त काग़ज़ के फूल में दिव्य मुद्रा अंगीकार करते हैं। हम देखते हैं कि सुरेश मुविंग डाॅली पर रखे एक सामान्य कैमरे से देवदास का एक दृश्य शूट कर रहा है। इस प्रकार काग़ज़ के फूल का स्थिर सिनेमास्कोप कैमरा न सिर्फ फिल्म युनिट की गतिविधियों को, देवदास के पात्रों को देख रहा है बल्कि बाद वाली फ़िल्म के गतिशील (अभिनय) उपकरण को भी देख रहा है। प्रत्येक वस्तु संकेतों को पकड़ती है। हालांकि, यदि गति जीवन को व्यक्त करती है तो, स्थिरता मृत्यु को। एक बार फिर से, सिनेमास्कोप फाॅरमेट का गहन संकेत बहुत साफ है। सिनेमास्कोप का आविष्कार खुली चैड़ी जगह को रिकार्ड करने के लिए हुआ था, अगर जरूरत होती है तो “सक्रिय भीड़” को फ़िल्माने के लिए। विडंबना यह है कि गुरुदत्त ने अधिकतर इनडोर शूटिंग के उपयोग से और बहुत कम सकारात्मक पात्रों को जोड़ते हुए एक आत्मीय कहानी समझने के लिए सिनेमास्कोप के अनिवार्य प्रकार्य को नष्ट करने का विकल्प चुना था। काग़ज़ के फूल अनिवार्यतः एक स्टुडियो फ़िल्म है जिसके बहुत कम दृश्यों की शूटिंग आउटडोर में हुई है। मेरा विचार है कि सुरेश के बढ़ते अकेलेपन, अलगाव और सूनेपन को अतिरंजित रूप में पेश करना ही इस व्युत्क्रम का कारण है। सिनेमास्कोप फाॅरमेट लोगों और वस्तुओं से अलगाव कीे हमारी चेतना को तीव्र करता है। नायक को “नायकत्व अलगाव” की ओर धकेलती है।
सिनेमास्कोप फ्रेम को एक ऐसे वर्ग की तरह देख सकते हैं जिसके “मध्य” भाग को छोड़कर, “ऊपर” और “नीचे” का भाग कटा हुआ हो। तब इस “मध्य” भाग को बढ़ा दिया गया हो। काग़ज़ के फूल में सुरेश निराशाजनक ढंग से (і)हिंस्र निर्माताओं और स्टुडियो हैक, (іі) पत्रकारों, (ііі) जनता, और (іअ) तीन औरतों (पत्नी, बेटी और प्रेमिका) के “मध्य” जकड़ लिया गया हो। इन तीन औरतों के साथ वह न तो रह सकता है और न ही उनके बिना रह सकता है। ई. एम. फोस्टर ने इसे “गड़बड़झाला” कहा है।
काग़ज़ के फूल के अलावा मैं सिर्फ़ ऐसी दो फ़िल्मों के बारे में जानता हूँ जिसमें सिनेमास्कोप और श्वेत-श्याम सिनेमाटोग्राफी एक साथ है। ये हैं, Froncois Truffaut की Jules et Jim (फ्रांस्कोप, 1961) और Jack Cardiff की सन्स एंड लवर्स (1962)। बाद की दोनों फ़िल्में क्रमशः Henri-Pierre Roche और डी. एच. लारेंस के आत्मकथात्मक उपन्यासों पर आधारित हैं। इन फ़िल्मों के निर्देशक क्रमशः अपनी कहानियों के केंद्रीय चरित्रों से काफी मिलते जुलते हैं। कहानियां भी काग़ज़ के फूल की तरह मजबूत नैतिक व्यंजना के साथ सुस्पष्ट स्मरणीय ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। तीनों फ़िल्में त्रिकोणीय मानव संबंधों का अध्ययन करती हैं जिनका हल मुश्किल है। हालांकि ये कथात्मक हैं लेकिन इनंका “वृत्तचित्र जैसा रूप” हंै। प्रसंगवश, फ़िरोज़ रंगूनवाला ने लिखा है कि काग़ज़ के फूल के सिनेमाटोग्राफर वी. के. मूर्ति ने Black Narcissus और Sons and Lovers के सिनेमाटोग्राफर Jack Cardiff के साथ अध्ययन किया था।
काग़ज़ के फूल गुरुदत्त के निजी नरक का दृश्यांकन है। इसीलिए श्वेत-श्याम रंगों का इस्तेमाल उपयुक्त है। मेरा अनुमान है कि इन रंगों का चयन फ़िल्म के यथार्थवाद को बढ़ाने के लिए किया गया है। दरअसल, उन्होंने मृत्यु की ओर अपनी स्थिर गति को दर्ज किया है, जो एक बार फिर हमें काग़ज के फूल के रूपक की ओर ले जाता है। सच्चे फूल भले ही वह श्वेत-श्याम ही क्यों न हो, वे अपने संदर्भ यानी दूसरे रंगों से (हमारी चेतना में) विलग नहीं होते। नकली होने के कारण काग़ज़ के फूल ऐसे रंगीन संदर्भों की मांग नहीं करते। रंग (विशेष रूप से हरा) पोषण/जीवन से जुड़ा होता है। इस प्रकार, फ़िल्म से रंग का अस्वीकार मरण और मृत्यु की ओर संकेत करता है। इसके अलावा, गुरुदत्त फ़िल्म में मजबूत नैतिक मुद्रा अपनाते हैं। वह दुनिया के झूठे उसूलों, असंवेदनशीलता और जर्जर पुरानेपन की निंदा करते हैं। श्वेत-श्याम का चयन ऐसे परीक्षण के लिए आदर्श है। फिर भी, उसको चुनकर भी वे उसका पूर्णरूपेण उपयोग करने से कतराते हैं। आॅर्थोक्रोमेटिक (लाल को छोड़कर सभी दृश्यमान प्रकाश के प्रति संवेदनशील श्वेत-श्याम फोटोग्राफिक फ़िल्म) स्टाॅक और प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था (जो श्वेत/श्याम टकराव को अतिरंजित करता है) का उपयोग करने की बजाए उन्होंने पेंक्रोमेटिक (स्पेक्टऊम के सभी दृश्यमान रंगों के प्रति संवेदनशील) स्टाॅक, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था (जो भूरी परछाई की ओर झुकी होती है) और यहां तक कि श्वेत-श्याम वैषम्य को कम करने के क्रम में सोफ्ट फोकस लेंस का चयन किया है। मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि बादशाह जहांगीर ने मरणासन्न इनायत खान का अधिकृत श्वेत-श्याम चित्र इसलिए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था क्योंकि वह दया से रहित था। तब कलाकार ने कुछ रंगों को जोड़कर चित्र को “हल्का” बनाया। गुरुदत्त ने अपने चयनित रंगों को अपनी तार्किक परिणति तक ले जाने से इन्कार क्यांे किया? आत्म-विनाश की ओर झुकाव के बावजूद मनुष्य अपने से प्यार करता है। इतना तो वह चाहता ही है कि उससे लोग प्यार करें। पर्दे पर यह उनकी मौजूदगी थी जो उन्हें कगार पर धकेल लायी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें करुणा, अवसाद भरे गीत और रूमानियत की रोशनी में याद किया जाए। उन्होंने याद करने की शर्तें खुद तय की। ऐसा प्रतीत होता है कि फ़िल्म (फ्रेम) के अंतर्गत (विश्व के लिए) आॅर्थोक्रोमेटिक/(स्वयं के लिए) पेंक्रोमेटिक रंगों को अंगीकार करने में वे नाकामयाब रहे। यही वजह है कि उन्होंने प्रत्येक को और प्रत्येक वस्तु को पेंक्रोमेटिक ग्रे में नहाया हुआ देखते हैं। काग़ज़ के फूल में यही अकेली समतावादी मुद्रा है जिसे वे पेश कर सकते हैं। दरअसल, यह समतावाद तकनीकी सीमाओं के चलते उन पर लादा गया था।
फोटोग्राफी आलोचक जेनेट मेल्कम का कहना था कि “श्वेत-श्याम छायांकन छायाकार से रंगों वाली दुनिया को ज्यादा गौर से देखने की मांग करता है जबकि रंगीन छायांकन उसे भूलने की अनुमति देता है”। क्योंकि वे यथार्थ का अमूर्तन करते हैं, श्वेत-श्याम फोटो भी दिमाग में अटक जाती है। बहुत से महान फोटोग्राफर- उनमें से Edward Weston, Henri Cartier Bresson, Alfred Stieglitz- इस बात पर जोर देते हैं कि रंगों का संबंध चित्रकला से है जबकि श्वेत-श्याम कला के रूप में फोटोग्राफी के ज्यादा अनुकूल है। ये टिप्पणियां स्थिर छायांकन से संबंधित हैं लेकिन ये सिनेमा पर भी लागू होती है। संभवतः गुरुदत्त काग़ज़ के फूल बनाने के लिए श्वेत-श्याम का उपयोग गंभीर (“कलात्मक”) उद्देश्य की ओर इंगित करने के लिए और निःसंदेह लंबे समय तक याद रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं।
काग़ज़ के फूल सबसे धीमी गति वाली हिंदुस्तानी फ़िल्मों में से एक है। जब कोई खरगोश ही नहीं है, तो कछुआ चाल वाली इस फ़िल्म को बनाकर गुरुदत्त कौन सी दौड़ जीतना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं होता। रफ़्तार इतनी धीमी है कि यह अनुभव होता है कि यह फ़िल्म दरअसल एक धीमी गति की फोटोग्राफी है। एक हद तक इसकी धीमी गति सुरेश के शराब से मंद पड़े दिमाग की ओर ध्यान खींचती है। इससे संबंधित दो मुद्दे हैंः (і) यह ज्यादा उचित होता कि फ्लैशबैक वाला हिस्सा धीमी गति से फ़िल्माया (फ़िल्म का अधिकांश हिस्सा मृत्यु की ओर बढ़ते सुरेश के दिवास्वप्न से संबंधित है) जाता और बिना फ्लैशबैक वाला हिस्सा सामान्य गति में बनाये रखा जाता, और (іі) यदि शराब सोचने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है तब वह उन्हें भी धीमा कर देता है। साफ तौर पर अतीत की स्मृति है। दरअसल वास्तविक जीवन के पियक्कड़ों में मंद गति और तीव्र स्मृति मानसिक दुर्बलता के विरुद्ध होती है। इसके अलावा शराब मनुष्य के सोचने की प्रकिं्रया को छिन्न-भिन्न कर देती है। इस बात की संभावना नहीं है कि उन्मत्त पियक्कड़ अतीत को साफ-साफ याद रखेगा और आख्यान आरंभ, मध्य और अंत के क्रम से प्रवाहित होगा। इस आलोचना को एक तरफ रख भी दें (मैं मान लेता हूँ कि सुरेश का मामला अलग है) तो भी धीमी गति के दूसरे पक्षों की खोज करना फायदेमंद होगा।
कहानी “अतीत की याद” के रूप में कही गयी है। बीते हुए क्षणों को स्मृति द्वारा पुनः अनुभव करना दरअसल “मृत समय” को अनुभव करना है। फ़िल्म के आरंभ में सुरेश कमोबेश मृत व्यक्ति के समान है। वह मरणासन्न लाश की तरह है जिसमें से सांस निकलने से पहले मृत क्षणों को याद करने से अधिक की शक्ति नहीं है। वह “निर्देशक की कुर्सी” पर बैठे हुए मर जाता है जो दो मौतों को संकेतित करता है, एक निर्देशक के रूप में और दूसरा व्यक्ति के रूप में। यह घटित होने से पहले क्षण-क्षण इस सीमा तक खींचा जाता है। कथानक से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण गीत (हमने देखी; वक़्त ने किया) जिनका बहुत समझदारी से उपयोग किया गया है, धीमी गति के गीत हैं। दोनों गीत ताल से रहित हैं (संकेतः मृत्यु में मेलाॅडी; जीवन तालबद्ध हृदय की धड़कनें हैं)। निश्चित ही वक़्त ने किया में जीवन की याद की प्रतिध्वनियां हैं (पियानो के नोटः सेलो पर Pizzicato) लेकिन यह वास्तव में मृत लय है। इसी तरह से फ़िल्म में तालबद्ध संपादन का अभाव है- यह भी फिर से मृतावस्था है।
Janet Malcom का कहना है कि “छायांकन की अद्वितीय क्षमता समय को बांध लेना है”। समय इतना घटना-पूरित होता है कि इसकी परीक्षा करने के लिए और इस पर ध्यान देने के लिए हमें फोटोग्राफी को धीमा करने की जरूरत होती है। धीमी गति को चुनने के पीछे गुरुदत्त संभवतः दर्शकों से सचेत अवलोकन हासिल करने की कोशिश करते हैं। “समय के घावों” के अनुभव से सिर्फ़ एक व्यक्ति को बरी किया गया है, और वह है सुरेश। सुरेश मोटे तौर पर फ़िल्म के अंतिम तीन चैथाई हिस्से तक बोतल हाथ में लिये रहता है। शराब का चेतना शून्य प्रभाव समय के पूर्ण अनुभव को कम कर देता है। दरअसल, शराब किसी को भी काल, दिक् और समाज से अलग कर देती है- मृत्यु से पहले एक प्रकार की मृत्यु। फिर भी, हम निर्देशक के तौर पर गुरुदत्त के आभारी हैं कि उन्होंने अपनी फ़िल्म की पीड़ादायक गति के पूर्ण अनुभव के अधीन अपने को कर लिया।
काग़ज़ के फूल का सबसे आकर्षक (और उत्कृष्ट) पक्ष इसका चीनी बाॅक्स संरचना है। यह समान मिथक- देवदास- पर फ़िल्म के अंदर फ़िल्म है। पिछले दशकों में कई बार वास्तविक जीवन में आधे-अधूरे या पूरे ढंग से यह मिथक कार्यान्वित हुआ है। फ़िल्मों में देवदास मिथक के स्तरों को मुझे गिनने देंः (і) मूल देवदास (1935; शीर्षक भूमिका में के. एल. सहगल के साथ निर्देशक पी. सी. बरुआ), (іі) देवदास का पुनर्निर्माण (1955; शीर्षक भूमिका में दिलीप कुमार के साथ निर्देशक बिमल राॅय), (ііі) काग़ज़ के फूल में सुरेश द्वारा निर्देशित देवदास, (іV) सुरेश स्वयं स्थानापन्न देवदास, और (V) गुरुदत्त का स्वयं के जीवन का उत्तरकाल जो कई रूपों में देवदास से मेल खाता है। एक मामूली से शराबखाने में जहां सुरेश देवदास शैली में शराब पी रहा है और ज़ौक़ की ग़ज़ल लायी हयात ए क़ज़ा गुनगुनाते हुए वह बरुआ के देवदास में सहगल की भूमिका की ओर संकेत करता है। उसी संगीत निर्देशक (एस. डी. बर्मन) का इस्तेमाल करते हुए और सुरेश की अभिनय शैली द्वारा भी वह बिमल राय के देवदास की ओर संकेत करते हैं। सुरेश भी दिलीप कुमार की तरह देवदास की भूमिका निभाता है। इसी दौरान अपने संक्षिप्त रूप में मिथकीय देवदास सहगल और बरुआ के जीवन में यथार्थ रूप धारण कर लेता है; दोनों ही ज्यादा शराब पीने से युवावस्था में ही मर गये थे। जो देवदास फ़िल्मों से लुप्त है वह मूल देवदास है जो शरतचंद्र चटर्जी के उपन्यास देवदास में है। क्यों? मेरे विचार में इसकी वजह यह है कि गुरुदत्त के (और हमारे) लिए सिनेमाई देवदास, ही सच्चा देवदास है, एक मिथकीय नायक। यह ध्यान देने की बात है कि शांति (वहीदा रहमान) सुरेश के लिए तब तक यथार्थ नहीं बनती जब तक कि वह उसे देवदास के रशेज देखते हुए उसे पर्दे पर नहीं देखता। इस प्रकार, यथार्थ वही है जिसका छायांकन किया जा सकता है। काग़ज़ के फूल (शिव के नृत्य की तरह) अपनी बहुआयामी अभिव्यक्तियों में मिथकीय (सिनेमाई) देवदास का नृत्य है। छायांकन के जादू से सिनेमाई देवदास औपन्यासिक देवदास को हजम कर जाता है। औपन्यासिक और सिनेमाई देवदास की तुलना और (विशेषतः) वैषम्य दिखाना ज्ञानवर्धक भी है और महत्त्वपूर्ण भी।
औपन्यासिक देवदास एक कथात्मक चरित्र था जो (і) दमनकारी सामाजिक-आर्थिक श्रेणीबद्धता (जाति व्यवस्था), (іі) दमनकारी पितृसत्ता के अनुपालन, और (ііі) माता-पिता द्वारा तय विवाह के प्रत्युत्तर में वह अपने आप को (स्वपीड़न आनंद) और जिनसे वह प्यार करता है (परपीड़न आनंद) उन सभी को नष्ट कर डालता है। शरतचंद्र का उपन्यास एक सामाजिक-राजनीतिक दस्तावेज है जो अपने पाठकों से अनुरोध करता है कि वह भारत में पुरातनपंथी दमनकारी परिस्थितियों के विरुद्ध उठ खड़े हों। वह उम्मीद करता है कि देवदास की अपने को नष्ट करने की इच्छा पाठकों में उससे उलट स्वतंत्र और अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था की इच्छा को पैदा करेगी।
देवदास के हर नये सिनेमाई रूपांतरण ने शरतचंद्र के अनिवार्य सामाजिक-राजनीतिक इरादों को अधिकाधिक विकृत और नष्ट किया है।
पी. सी. बरुआ के देवदास में नायक के स्याह आत्म-विनाशक प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि बरुआ ने क्यों पुस्तक के सामाजिक-राजनीतिक आयाम पर मौन रहना अंगीकार किया। प्रमथेशचंद (“प्रिंस”) बरुआ दरअसल गौरीपुर (आसाम) के राजा के बेटे थे। उन्होंने सामंती कुलीन वर्ग के पतन को देखा था। वह ऐसे राज्य के “प्रिंस” थे जिसका अब अस्तित्व नहीं रहा था। वह अपने वर्ग की मौत का शोक मना रहे थे। देवदास उसी वर्ग का प्रतिनिधि है। सामंती कुलीन वर्ग के मरण के विलाप के दौरान उन्होंने (सिनेमा के शक्तिशाली माध्यम के जरिए) कामयाबी से (पार्वती और चंद्रमुखी सहित) उन साधारण लोगों के मन में सहानुभूति पैदा कर दी जो स्वयं उस कुलीन वर्ग से उत्पीड़ित थे। बरुआ की देवदास अपने स्याह-माधुर्य के साथ एक प्रतिक्रियावादी फ़िल्म है।
सभी तरह का सिनेमा बीते वक्त की याद (नाॅस्टेल्जिया) होता है। बिमल राय का देवदास बीते वक्त की याद की याद (नाॅस्टेल्जिया आॅफ नाॅस्टेल्जिया) है। हम इस बात को याद कर सकते हैं कि प्रिंस बरुआ के देवदास के लेंस के पीछे सिनेमाटोग्राफर बिमल राय की आंख थी। उनका अपना देवदास उनके युवा दिनों के बंगाल की खट्टी-मीठी, करुण और नाॅस्टेल्जिक यात्रा है, वह बंगाल जो अब खो चुका है (बिमल राय उस बंगाल के रहने वाले थे जो पूर्वी पाकिस्तान में बदल चुका था और बाद में जो बांग्लादेश के रूप में उभरा था)। यदि उनकी युवावस्था के बंगाल में सामाजिक-राजनीतिक समस्याएं थीं, तो, उन्हें धूप-छांव के आकर्षक हल्के-फुल्के खेल की तरह पेश किया गया था। देवदास अब एक सपने के खोने का प्रतीक बन गया है। बिमल राय की फ़िल्म भी अपने चारों ओर की सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकता से देवदास की निरंतर विमुखता को पेश करती है। देवदास में निजबद्धता बढ़ती जाती है। इस निजीकरण को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए तब के भारत के “ट्रेजेडी किंग” दिलीप कुमार का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उन्होंने देवदास में बहुत संयमित (“बंगाली” किस्म के अभिनय) अभिनय किया लेकिन यह उनकी प्रतिभा और भारतीय “वितराग भाव से मोह” ही था जिसने कि देवदास के “असमाजीकरण” को पूर्णता दी। दरअसल, फ़िल्म के अंत में बिमल राय ने देवदास को एक ऐसी छलावे वाली रेलगाड़ी में बैठा दिया जो कहीं नहीं पहुंचाती। खून की उलटी करने वाले देवदास से पहले वाला देवदास गुरुदत्त को त्रस्त करता रहता है। यही वह देवदास है जिसे उन्होंने काग़ज़ के फूल में अपहृत कर लिया था। बाद वाली फ़िल्म अपनी अंतिम यात्रा पर निकले देवदास के चिंतन और विषाद के बारे में है। चिंतन और विषाद उसकी पीड़ा को और बढ़ा देता है, यहां तक कि उसको पूरी तरह से तोड़ डालता है।
यहां मैं Orson Welles की फ़िल्म सिटिज़न केन की याद करना चाहूंगा जिसके एक दृश्य में केन अपनी इस्टेट ज़ानाडु के एक बरामदे में से गुजर रहा है जहां आमने-सामने दर्पण लगे हुए हैं। जब वह दर्पणों के बीच से गुजर रहा है तो उसकी छवि विखंडित हो जाती है और अनगिनत भी हो जाती है। छवि एकाकी जीवन में विनाश के स्तरों को कई गुना बढ़ा देता है।
निश्चय ही देवदास के शून्यवादी पहलू के गुरुदत्त के दृष्टिकोण में भव्यता निहित है। इसके अलावा, वह निष्कपट भाव से देवदास के हाव-भाव के एक स्तर को निर्मित करते हैं और स्वयं ही दूसरे स्तर में डाल देता है। फिर भी, गुरुदत्त काग़ज़ के फूल में देवदास के मिथक के टूटे-फूटे स्तरों में निहित संभावना का पूर्णरूपेण उपयोग करने में नाकामयाब रहे। मैं अब इस दृष्टिकोण का औचित्य बताने जा रहा हूँ।
काग़ज़ के फूल में देवदास और उसका स्थानापन्न (सुरेश) समाज से अलग हो जाते हैं। सुरेश द्वारा बनाई जा रही देवदास फ़िल्म में हम देखते हैं कि देवदास एक गंदी सी गली में शराब पिये हुए पड़ा है जहां संयोग से पार्वती आ जाती है। ‘देवदास’ का मुख्य चरित्र चंद्रमुखी सुरेश और गुरुदत्त दोनों की फ़िल्मों से गायब है। वहां वर्ग संबंधी अंतर की ओर संकेत किया गया है। उदाहरण के लिए, उससे विमुख पत्नी उच्चवर्ग से है जबकि शांति का संबंध गरीब परिवार से है। गुरुदत्त इन भेदों के महत्त्व पर अधिक ध्यान नहीं देते। ये बस “प्रसंगवश” दी गयी सूचनाएं हैं। इस प्रकार देवदास के समाजिक-राजनीतिक संदर्भ को सरलीकृत करते हुए वे नायक की निजी दुर्दशा पर टूट पड़ने के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर भी, इस समाजिक रूप से कंगाल दुनिया में सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण का महत्त्व है।
काग़ज के फूल का सामाजिक संसार नायक केंद्रित (गुरुदत्त केंद्रित) है। नायक के इर्दगिर्द दो वृत्त हैंः सूक्ष्म-सामाजिक (पत्नी, पुत्री और प्रेमिका) और स्थूल-सामाजिक (विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता)।
सूक्ष्म-सामाजिक इकाई पूरी तरह से स्त्रियों से निर्मित हैं। गुरुदत्त इन सबको नकारात्मक रूप में देखते हैं। रंजिशज़दा पत्नी उच्च वर्ग की लड़ाकू और ओछी औरत है (क्या ऐसा सोचना अनुचित है कि वह गीता दत्त का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि निर्देशक की रंजिशज़दा पत्नी है?)। पम्मी किशोर वय की बेटी है जो अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ेगी। शांति के प्रति अपने पिता के बढ़ते प्यार में बाधा डालने के लिए वह मुश्किलें बढ़ा देती हैं जिसका नतीजा पिता के पतन में निकलता है। वह सुरेश के जीवन में अंधेरा भरने का काम करती है। एकबार जब उसके पिता विस्मृति में चले जाते हैं, तो वह गायब हो जाती है। वह एक “स्याह फरिश्ता” है। शांति ही एक अकेली इंसान है जो सुरेश को समझती है। उन दोनों के बीच भावनात्मक और कलात्मक सहभागिता है। अपनी सती-सावित्री छवि को स्थापित करने के लिए वह पम्मी से वादा करती है कि वह सुरेश के साथ अपने संबंध को तोड़ देगी। उसके बाद वह दिग्भ्रमित हो जाता है। इस दौरान गुरुदत्त शांति के लिए भयावह विरोधाभासी स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर वह पम्मी की मांग को बिना किसी विरोध के स्वीकार नहीं करती तो वह पार्वती के आदर्श पर खरी नहीं उतरती। और तब निश्चय ही सुरेश की नज़र में (और भारतीय दर्शकों की नज़र में भी) वह मूल्यहीन होती। स्त्री जंजीरों में जकड़ी हुई है। उसे पार्वती बनने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि देवदास को विस्मृति में भेजा जा सके। शांति की भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है जो गुरुदत्त के वास्तविक जीवन की “आकांक्षा” है। यह विडंबना नही ंतो क्या है कि (सुरेश से) उसके अलगाव का गीत (वक़्त ने किया) गुरुदत्त के वास्तविक जीवन की रंजिशज़दा पत्नी (गीतादत्त) ने गाया है। यह क्या है, पहेली?
फ़िल्म में वहीदा रहमान ही अकेली पात्र है जिसने दोहरी भूमिका निभायी है, शांति और पार्वती की। संभवतया यह दोहराव उसके द्वारा नायक को छोड़ने की तीव्रता जताने के लिए उस पर थोपा गया है। इससे भी बदतर यह है कि उसकी नकारात्मकता इस तथ्य से बढ़ जाती है कि वह (“सृजित”) अपने ही सर्जक का परित्याग करती है (यहां “एक सितारा पैदा हुआ” से कुछ ज्यादा ही है)। अभिनेत्री एक ऐसे कर्ज से जकड़ी हुई है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। या यह कहना ज्यादा सही होगा कि जिसे चुकाने की उसे अनुमति नहीं है।
गुरुदत्त और शांति (वहीदा रहमान) के बीच के संबंध समान स्तर के नहीं है। यह उनके बीच के लेनदेन से स्पष्ट हो जाता है। जब वे अंधेरी बरसात की रात में पहली बार मिले तो सुरेश ने अपने ओवरकोट से उसके पूरे शरीर को ढंक दिया था। बदले में वह उसे मामूली सा स्वेटर ही दे सकती है (जो उसकी छाती को ही ढक पाता है)। बाद में जब सुरेश अपने जीवन में पूरी तरह पस्त हो चुका होता है तब हम उसे वही स्वेटर पहने हुए देखते हैं जिसमें लगभग पचास छेद होते हैं और जिसके प्रत्येक छेद में से मौत तेजी से अंदर जा रही होती है। शांति उसकी उदारता की बराबरी नहीं कर सकती।
जहां तक स्त्रियों के साथ सुरेश के संबंधों का सवाल है, यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि उसका किसी के साथ यौन संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी बेटी के जन्म के बाद उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है। न तो उसका अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध है और न ही शांति के साथ। अब, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को संसार या जीवन से जोड़े जो किसी स्त्री (या स्त्रियों) के साथ जुड़ने पर होता है। प्रेम की चाह ही रूमानी प्रेम को “आकार देती है”, जिसकी परिणति (इच्छा के रूप में ही सही) जीवन के पुनरुत्पादन में होती है। सुरेश ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब उसमें ऊर्जा का संचार असंभव है। इसके अलावा, उसकी अकेली संतान एक लड़की है इसलिए उसका नाम उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जायेगा।
उसकी चीख में से एक ही आवाज़ निकलती है, “देखो! मैं औरतों का सताया हुआ हूँ”। यह जानना शिक्षाप्रद होगा कि फ़िल्म में “औरतें” किसका प्रतीक हैं। वे हिंदू चेतना में पृथ्वी (“धरती माता”) की प्रतीक हैं। दरअसल, गुरुदत्त अपने अस्तित्व के प्रति विद्वेष के लिए पृथ्वी को दोषी करार देते हैं। पृथ्वी ने उनका परित्याग कर दिया है। उनके तर्क में इतनी ताकत होती है कि हमारे लिए उसके विपरीत देखना कठिन हो जाता है। यह इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि गुरुदत्त के चश्मे से हमें धरती स्याह नज़र आती है।
यह समझना बिल्कुल सही है कि गुरुदत्त यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत गौण है। हालांकि शांति के साथ व्यवहार के मामले में सुरेश उस समाज से बेहतर नहीं है जिसकी कि आलोचना की जा रही है। सुरेश उस पर राजसी कानून लागू करता है। वह शो-आॅफ पार्टी में जाने के लिए उसे (यहां तक कि बालों के संवारने के तरीके के लिए) फटकारता है। अगले दृश्य में? शांति पार्वती है जो भारतीय स्त्री की परंपरागत सती सावित्री छवि का प्रतिनिधित्व करती है। शेर पूरी सुरक्षा के साथ पिंजरे में चला जाता है।
वैंपायर को एक ऐसे प्राणी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है जो “मर कर भी नहीं मरता”। मृत्यु के बाद वह इंसानों विशेषतः उन औरतों का खून चूसकर पुनर्जीवित हो जाता है जो उसका प्रतिरोध नहीं कर पाती। “रात के राजकुमार” को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए औरतों के हरम की जरूरत होती है। हिंदुस्तानी सिनेमा के प्रिंस बरुआ का मिथकीय देवदास ऐसा ही वैंपायर प्रतीत होता है (ये देवदास फ़िल्में कितनी अंधकारपूर्ण हैं!)। एकबार फ़िल्म रिलीज होने के बाद वह कई पीढ़ियों की (पार्वती और चंद्रमुखी और उन जैसी) औरतों को अपना भोजन बनाता प्रतीत होता है। थोड़े-थोड़े समय बाद अपनी इस हवस को पूरा करने के लिए पर्दे से बाहर छलांग लगाता है। उसे हमेशा बिना किसी तरह का प्रतिरोध किये उत्पीड़ित स्त्रियां तैयार मिलती हैं।
इसके अलावा, गुरुदत्त संसार की सनक से अपनी रक्षा करने में नाकामयाब रहने के लिए औरतों का तिरस्कार करते प्रतीत होते हैं। यह संसार उत्पीड़ित स्त्रियों के वृत्त के बाहर अवस्थित है। यह संसार लालची निर्माताओं/स्टूडियो मालिकों, शातिर प्रेस, संवेदनहीन जज, और ढुलमुल (यहां तक कि हिंसक) लोगों (अर्थात दर्शकों) से मिलकर बना है।
सिर्फ एक व्यक्ति जो इस नकारात्मक धारणा से बच पाया है (वह भी कुछ शर्त के साथ) वह है सुरेश का मुस्लिम ड्राइवर। वह अपने मालिक की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। वह कैसे कामयाब हो सकता था? वह उतना ही अच्छा था जितना कि नाश्ते में खाया गया कबाब। गुरुदत्त उसे पेट्रोल स्टेशन के मालिक में बदल देता है। एक मुस्लिम ड्राइवर द्वारा सुरेश को बचाने की अनुमति देने का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि इससे कठिनाइयां पैदा होतीं।
हालांकि गुरुदत्त ने काग़ज़ के फूल में एक अराजनीतिक मुद्रा अख्तियार की है, फिर भी सामाजिक इकाइयों की गत्यात्मकता बताती है कि वे राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियावादी हैं। उनकी राजनीति दमन और विनाशवाद की ओर संकेत करती है। एक निर्देशक जिसका जनता में बिल्कुल विश्वास नहीं है और जो आत्म-विनाश से आगे भविष्य नहीं देख पाता, उसका कोई सामाजिक-राजनीतिक महत्त्व नहीं होता (या सीमित होता है)। सामाजिक कार्यकत्र्ता Eldredge Cleaver ने कहा था, “अगर आप समाधान के हिस्से नहीं हैं तो आप समस्या के हिस्से हैं”। गुरुदत्त को इसके सिवा कोई समस्या नज़र नहीं आती कि वह अपने नायक (और खुद) को मृत्यु की ओर भेज दे। वह दुनिया से यही चाहता है कि वह उसके अलगाव और मौत की गवाह बने। इस बीच, वह सभी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। उसका मानवद्रोह बहुत चिंताजनक है। प्रेस और जनता को असहानुभूतिपूर्ण ढंग से दिखाकर वह उन्हें अपराधबोध में बांध देता है। इसी वजह से उसके कार्य को निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से देखना संभव नहीं रहता। यदि ऐसी कोशिश की भी जाती है तो यह डर बना रहता है कि वह कहीं हमें ही दोषी न ठहरा दे। अपनी नज़रे फिराकर ही हम भूसे में से बीजों को अलग कर सकते हैं। यही करना होगा। हमें उसके प्रति ईमानदार होना होगा क्योंकि वह हमारे प्रति ईमानदार नहीं है। उनकी फ़िल्मों को जरूरत से ज्यादा महत्त्व देने से अपने को रोकना होगा क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है।
तथ्य यह है कि गुरुदत्त वैयक्तिक कलाकार के लिए किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते। काग़ज़ के फूल में वे सुरेश के रवैए की वैध आलोचना को भी स्वीकृति नहीं देते। सामाजिक संदर्भ में दीवानापन, यहां तक कि सर्जनात्मकता भी अर्थहीन है। सुरेश किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी के साथ किसी तरह के संतोषप्रद सामाजिक-राजनीतिक सहमति पर नहीं पहुंचता। चाल्र्स डिकन्स की तरह गुरुदत्त की “समाज की आलोचना भी कमोबेश नैतिक ही है। इसी वजह से, उसके कार्य में कोई रचनात्मक सुझाव निहित नहीं होता” (जार्ज आरवेल)। वस्तुतः वह उन सामाजिक परिस्थितियों की पुनर्रचना करता है जो विनाश की ओर ले जाती है। सच्चाई यह है कि गुरुदत्त मृत्युकामी थे। व्यावसायिक सिनेमा के बाहर (जिसे वह नापसंद करते थे) ऐसा प्रतीत होता है कि वे “अपनी तरह का सिनेमा” बनाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाये। सिनेमा एक लोकतांत्रिक कला है। यहां तक कि वे लेखक-फ़िल्मकार भी जिनका अपनी फ़िल्म पर पूरा नियंत्रण होता है उन्हें भी फ़िल्म बनाने के लिए दूसरे लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है। अपने दौर में ख्वाजा अहमद अब्बास ने सामाजिक मूल्य की छोटी फ़िल्में बनायी थी। सच्चाई यह है कि गुरुदत्त सिनेमा में शून्यवादी “रचनात्मक” निरंकुशता चाहते थे। इसलिए उनके साथ चलना मुश्किल था।
इनके अलावा भी, काग़ज़ के फूल अपनी औपचारिक उत्कृष्टता की दृष्टि से देखने पर भी दोषपूर्ण नज़र आती है। जो अमेरिकी मेरे साथ यह फ़िल्म देख रहे थे, फ़िल्म देखने के दौरान मुझे गुस्से से देख रहे थे और हम सभी बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। हम जान गये थे कि हम एक मामूली फ़िल्म देख रहे हैं (ज्यादा से ज्यादा) जो चतुर बनने की कोशिश कर रही है। काग़ज़ के फूल के सभी संकेत नष्ट हो गये थे क्योंकि वे जर्जर सिनेमाई वाहन पर टिके हुए थे। देवदास मिथक के बहुत से स्तरों को एक दूसरे के मुकाबले में रखना एक चतुराई भरा विचार था। लेकिन उसका मकसद क्या था? प्रत्येक देवदास को दूसरे के साथ यदि बहस में रखा जाता तो वह कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण होता और उससे कुछ मुक्तिकामी संदेश भी हासिल होता। वह देवदास मिथक को द्वंद्वात्मक दृष्टि से जांचने में असफल रहे। यह गुरुदत्त नहीं कर सकते थे क्योंकि खेदजनक ढंग से सिनेमाई शिल्पकारिता में उनकी प्रवीणता बहुत सीमित थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन कोई काग़ज़ के फूल को ज्यां लक गोदार की फ़िल्म Le Mapris (कंटेप्ट) के साथ देखकर गुरुदत्त की असफलता की गहराई का मूल्यांकन कर सके। काग़ज़ के फूल की तरह गोदार की फ़िल्म (і) फ़िल्म के अंदर फ़िल्म है, (іі) एक फ़िल्मकार के बारे में जिसका निर्माताओं से झगड़ा है, (ііі) शादी टूटने के बारे में है, (іअ) हमारे समय में नैतिक भ्रष्टाचार को तर्कसंगत ठहराने के लिए एक प्राचीन मिथक (युलिसिस जिसका निर्देशन Fritz Lang ने किया है) को अपमानित किया गया है, और (अ) मौत के बारे में है। गोदार ने जहां तक संभव हुआ है, आधुनिक विश्व में हमारी अरक्षितता को समझने के लिए मिथक और यथार्थ के बीच द्वंद्वात्मकता को स्थापित किया है। Le Mapris एक संपादक का दुःस्वप्न है और फिर भी, विश्व के बारे में पीड़ाजनक अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हिस्से को लगभग दोषरहितता के एक साथ रखा गया है। गोदार मुक्त हो गये। उन्होंने हाॅलीवुड की निर्माण व्यवस्था के अंतर्गत फिर कभी काम नहीं किया। वे बाद में प्रभावशाली फ़िल्में बनाते रहे। लेकिन गुरुदत्त की मौत हो गयी।
काग़ज़ के फूल में जो भी आख्यान वे कहना चाहते थे, उसके कहने के लिए वे इधर-उधर भटकते रहे और इस तरह विपुल मात्रा में उन्होंने फुटेज की बरबादी की। जाॅनी वाकर से संबंधित पूरी उपकथा गैर जरूरी थी। विषय से जुड़े दो गीतों (हमने देखी; वक़्त ने किया) को छोड़कर शेष फुटेज का “दिखावे के लिए किया गया व्यय” है। नायक का अपनी पत्नी से अलगाव का आधार बहुत खोखला है। शांति एक अविश्वसनीय घुमंतू चरित्र (उसका कोई परिवार नहीं है) है। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में ऐसी खूबसूरत आज़ाद औरतें कितनी होंगी। अनगिनत असंभव संयोग दर्शक की साख पर आघात करना है। सुरेश को छोड़कर, शेष सभी चरित्र जोड़तोड़ कर बनाए गए एकआयामी हैं। अबरार अल्वी के संवाद अत्यंत साधारण है। सिनेमा में बोले जाने वाले शब्द फ़िल्म के मौन को भी आवाज़ देने वाले होने चाहिए। अल्वी के शब्द मौन को भी मार देते हैं। जो थोड़ा बहुत मौन बचा भी रहता है उसे घटिया पाश्र्व संगीत विरूपित कर देता है। एस. डी. बर्मन के दो गीत (हम ने देखी; वक़्त ने किया) प्रथम श्रेणी के है। वक़्त ने किया प्रेरणास्पद संरचना है जिसे अत्यंत उत्कृष्टता के साथ संयोजित किया गया है। दूसरे गीत फालतू हैं। माक्र्सवादी शायर कै़फ़ी आज़मी ने यहां गैरमाक्र्सवादी वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गुरुदत्त को यह आश्वस्त कर दिया है कि “यह भी करेंगे और वह भी करेंगे”। ज़ौक़ की ग़ज़ल “लायी हयात ए क़ज़ा” शानदार है। वी. के. मूर्ति का छायांकन आश्चर्यजनक ढंग से अच्छा है। कुछ दृश्य स्मरणीय हैं। खासतौर पर अंतिम दृश्य जब सुरेश की मृत्यु होने वाली होती है, पर्दे पर फ्ल्डलाइट की तेज रोशनी फ़िल्म को “कुरबान” कर देती है। यह काग़ज़ के फूल की चिता है।
भारत के गरीब को क्रूर सनक के साथ बर्ताव किया जाता है। एक सुबह शांति गाँव में गरीब बच्चों के लिए गाना गा रही हैं; दूसरे दृश्य में वह उन्हें छोड़ देती है। एक बेहूदा गीत में वह वह “गरीबी हटाओ” के नारे को विरूपित कर रही होती हैं। विनोबा भावे को इस चमत्कार को देखना चाहिए।
काग़ज़ के फूल के प्रदर्शन के 27 साल बाद गुरुदत्त के काग़ज़ के फूल मुरझा चुके हैं।
1986
आभार
विजयलक्ष्मी देसराम के साथ विचार विमर्श और प्रोत्साहन के बिना यह लेख नहीं लिखा जा सकता था। उनके सहयोग के लिए धन्यवाद!
यह लेख दिवंगत गुरुदत्त की स्मृति को समर्पित।
संदर्भ
Bannerji Shampa, 1985. Profiles : Five Film-Makers from India. National Film Development Corp.; New Delhi
Cameron Ian. 1987. The Films of Jean Luc Godard. Studio Vista Ltd. London.
Malcom Janet. 1980. Essays on the Aesthetic of Photography—DIANA & NIKON. Davod R. Godine, Publ; Boston.
Orwell George. 1946. Dickens, Dali and Others. Harcourt Brace Jovanovich, Inc; New York.
Rangoonwalla, Feroze. 1973. Guru Dutt. National Film Archive of India, Poona.
Santog, Susan. 1979. On Photography. Dell Publ. Co. Inc; New Delhi.
(अशरफ़ अज़ीज़ की पुस्तक ‘हिंदुस्तानी सिनेमा और संगीत’ अनुवाद : जवरीमल्ल पारख, 2022, ग्रंथशिल्पी से साभार)