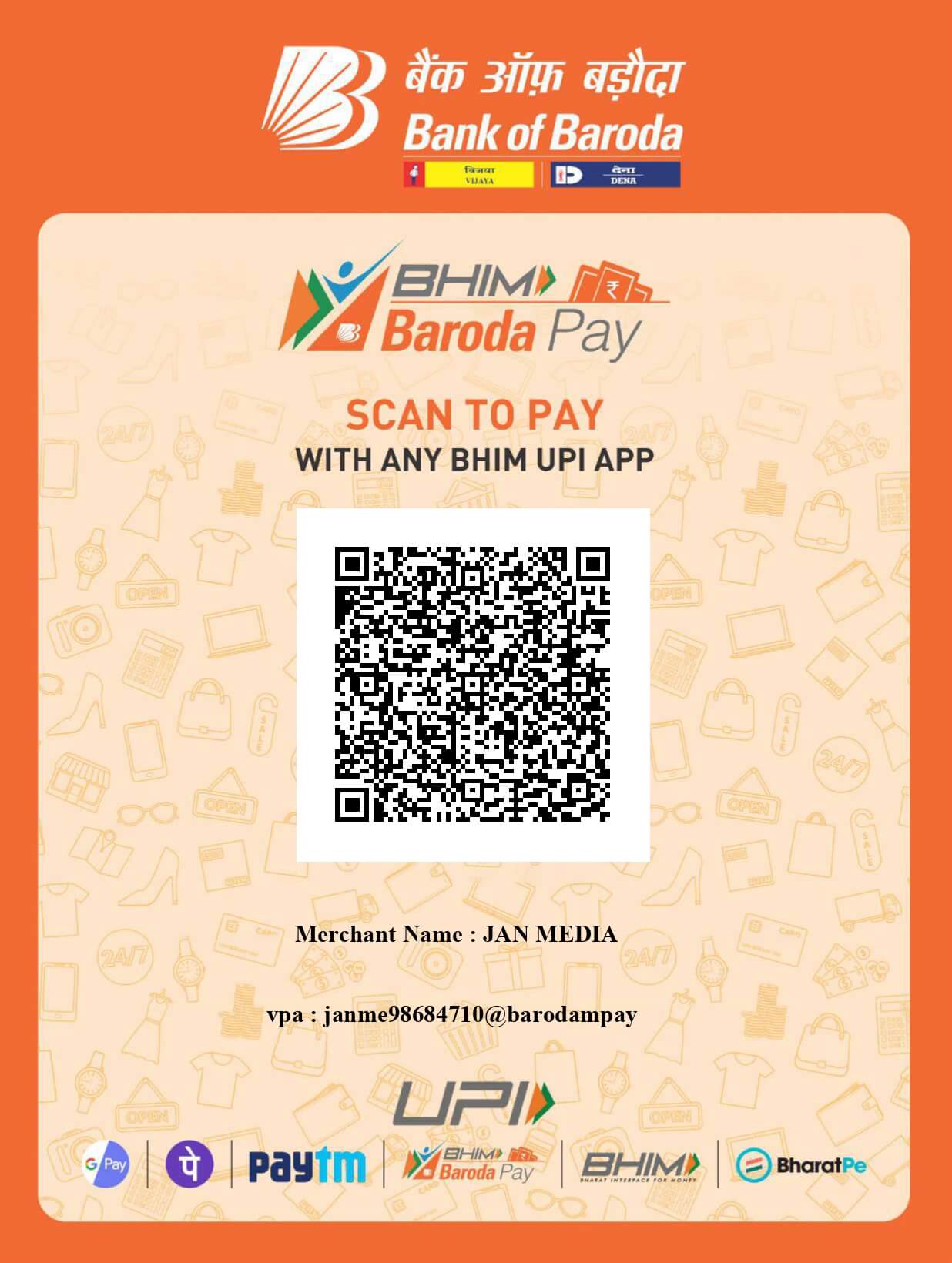सवाल यह उठता है कि क्या डिजिटल तकनीक की इतने बड़े पैमाने पर तैनाती हमें वास्तव में सुरक्षित बनाती है, या यह केवल सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है, बस. परियोजना विकास के दृष्टिकोण से भी भारत जैसे गरीब देश के लिए क्या यह खर्च उचित है? आज की बैठक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इससे हमें न्याय का अवसर मिलता है?
“न्यायाधीशों को क्या पता है कि हम कंप्यूटर को नहीं बता सकते?”
मेरा मानना है कि दो दशक पहले उभरे रुझानों से कुछ जवाब मिल सकते हैं. जब दिसंबर, 2003 के अंत में देश में ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) की पहुंच क्रमशः 0.02%, 0.4% और 0.8% थी,उस समय आपराधिक न्याय सुधारों पर गठित न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने दो प्रमुख मुद्दों की पहचान की थी: लंबित आपराधिक मामलों की एक बड़ी संख्या और उनके निपटान में लंबी देरी, साथ ही गंभीर अपराधों के लिए दोषसिद्धि की कम दर. इस समिति ने प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत की, “यदि अपराध की मौजूदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना है, तो न केवल जांचकर्ताओं की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, बल्कि उन्हें उन्नत तकनीक में प्रशिक्षित करना होगा”. इसकी अन्य सिफारिशों में पुलिस के लिए “खुफिया उपकरण और डेटाबेस विकसित करना और साझा करना शामिल है, जो मामलों की जांच और अभियोजन में मदद करेगा”. अंतिम पृष्ठ पर रिपोर्ट का समाप्ति इस अनुशंसा के साथ होती है, “समाज बदलता है, इसलिए इसके मूल्य भी बदलते हैं. तकनीक में बदलाव के साथ अपराध विशेष रूप से बढ़ रहे हैं.”कुछ साल बाद आपराधिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर माधव मेनन समिति की रिपोर्ट पुलिसिंग ब्यवस्था में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रत्याशित प्रभावों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है. रिपोर्ट में “इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और वैज्ञानिक साक्ष्य के उपयोग” पर एक अलग अध्याय शामिल है और यह दर्ज किया गया है कि “विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) के विकास से अपराध और न्याय परिदृश्यों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपराध की समस्याओं और चुनौतियों को और अधिक कुशलता से हल करने में मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से तकनीकी उपकरणों की मदद से किये जाने अपराधों के मामले में. प्रौद्योगिकी एक अवसर हो या जोखिम, दोनों ही रूप में राज्य की भूमिका को उजागर करता है, जिसमें पुलिस और न्यायिक प्राधिकरण मुख्य संस्थानों के रूप में शामिल हैं. हितधारकों की भी भूमिका है.ये अवधारणा प्रौद्योगिकी के पक्ष में एक पूर्वाग्रह को भी दर्शाता है, जो इस अर्थ में निर्धारणवाद का एक रूप है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने से आपराधिक जांच और परीक्षण की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, दक्षता और प्रभावशीलता आती है. मेरा मानना है कि इस तरह के विचार में दूरदर्शिता का अभाव है क्योंकि हम जानते हैं कैसे पुलिस के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का क्षरण करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. मुझे संदेह है कि कानूनी दिग्गजों की अध्यक्षता वाली इन समितियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापकों में से एक की बहस को पढ़कर कोइ फायदा उठाया है, यह प्रौद्योगिकी बुत का तार्किक निष्कर्ष है. जिसमें जॉन मैकार्थी ने उत्तेजित होकर कहा, “न्यायाधीशों को क्या पता है कि हम कंप्यूटर को नहीं बता सकते?”
नीतिगत दस्तावेज अपने आप व्यवहारिक वास्तविकताओं में नहीं बदल जाते. इसलिए, यह स्पष्ट है कि पुलिसिंग के लिए डिजिटल तकनीकों का प्रावधान उनके विकास और उपलब्धता के बिना नहीं किया जा सकता है.निजी उद्योग ने इस अवधि के दौरान जरूरत पड़ने पर कभी-कभी इसकी तरफ कदम बढ़ाया है. मनीषा सेठी ने अपनी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी फेयर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं द्वारा निगरानी तकनीकों की की गईं पेशकश का विस्तृत विवरण दिया है. वे आगे नोट करती हैं कि फिक्की टास्क फोर्स ने 2008 में दुखद मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में “इनवेसिव तकनीक” को प्रमुखता दी थी. FICCI और अर्नस्ट एंड यंग के अनुसार, स्मार्ट और सुरक्षित शहरों की नींव है, “केंद्रीकृत डेटा सिस्टम, GIS-आधारित विश्लेषण और रिपोर्टिंग, और CCTV कैमरों से देशव्यापी सर्विलांस तकनीक.” आज, यह प्रौद्योगिकी नियतत्ववाद केवल “भविष्यदर्शी पुलिसिंग” जैसे वाक्यांशों के साथ नीति शब्दावली में प्रवेश कर रहा है. लेकिन, इससे पहले कि हम इन जादुई सामानों में कदम रखें, मेरा मानना है कि हिंसास्थलों पर डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुलिस की प्रतिक्रियाओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है.
गाजीपुर लैंडफिल से भी ज्यादा जहरीला
यहां, 23 से 26 फरवरी, 2020 के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को डिजिटल पुलिसिंग और आपराधिक न्याय की भूमिका के संदर्भ में एक केस स्टडी के रूप में लिया जा सकता है. दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई एक आरटीआई के जवाब के अनुसार इसके परिणामस्वरूप कुल 53 मौतें हुईं और 581 घायल हुए, जिसमें 754 प्राथमिकी और 1369 गिरफ्तारियां हुईं. दिल्ली में अनुमानित 2.8 कनेक्शन प्रति व्यक्ति के उच्च टेलीघनत्व का मतलब था कि कई निवासी घटना के समय फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे. इन घटनाओं के पीछे नफरती और भड़काऊ भाषणों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है. कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप की एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अक्सर हिंसा के एपिसोड का निहित हिस्सा होता है, चाहे वह झूठी अफवाहें फैलाकर, आपत्तिजनक भड़काऊ ट्रॉप को फैला करके, या हिंसक कार्यों को आसान बनाने के माध्यम से हो.”
मेरा मानना है कि सोशल मीडिया एक सर्वव्यापी डिजिटल मीडिया इकोलॉजी का एक केंद्रीयबिंदु है. यह एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है. जिनके परिणाम स्वरूप फरवरी की घटनायें हई उन नफरती और भड़काऊ भाषणों के चक्र को पूरी तरह से समझने के लिए व्यापक डिजिटल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है क्यांकि यह तेज गति वाला है, हमेशा मौजूद रहता है और हमारे विचारों को प्रभावित करता है. यह पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर कनेक्टिविटी, एल्गोरिदम द्वारा संचालित होता है जो हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को हैक कर लेता है. यह गुटों का निर्माण करता है और हमारी सोच के निकट की आदिवासीवादी प्रवृत्तियाँ पैदा करता है. यहां भाषण और सेंसरशिप दोनों के शक्तिशाली उपकरण, जो कानूनी और तकनीकी हैं, लगातार उन सूचनाओं को क्यूरेट करते रहते हैं जो हमें मिलती रहती हैं. अंतत: यह हमारी समझ को कुंद कर देता है.ऐसा है इसका सम्मोहन समाज को हिंसा में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर देता है. लोग इसके नुकसान को स्पष्ट रूप से देखते हैं फिर भी वे अपनी मदद नहीं कर सकते. वे इसे “नरक स्थल” तो कहते हैं, लेकिन वे इसके निवासी बने रहने का चयन हर रोज़ करते हैं. यह गाजीपुर के शहरी कचरे के लैंडफिल के समान है, जो लगातार जलती रहती है और जहरीला धुंआ छोड़ती रहती है. फिर भी, हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं. लेकिन अपने फ़ीड को ताज़ा करते हैं और हर पल अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, एक नर्वस पिस्सू की तरह.
विडम्बना यह है कि डिजिटल मीडिया के जिस बाढ़ का हम सामना करते हैं, उसकी भी गुणात्मकता के आवश्यकता अनुसार राशनिंग की जाती है. विशेष रूप से भारत जैसे उत्तर-औपनिवेशिक समाजों में, सेंसरशिप ने संचार माध्यमों को नियंत्रित करना जारी रखा है. यहां सूचनाओं को पूरी तरह ब्लैकआउट किया जा सकता है. इन्हें आमतौर पर इंटरनेट शटडाउन कहा जाता है और यह इंटरनेट शटडाउन सेंसरशिप का सबसे गंभीर रूप है. भारत में न केवल सीमावर्ती राज्यों में ही बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में भी यह अमल में लाया जाता है. उदाहरण के लिए, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के दौरान सरकार ने इंटरनेट बंद नहीं किया था, लेकिन गणतंत्र दिवस पर किसान आन्दोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया था. यहां, सबूतों की अक्सर अवहेलना की जाती है. बड़े पैमाने पर हिंसा के दौरान इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव इरादे के विपरीत प्रति-उत्पादक हो सकता है, क्योंकि शोध से पता चला है कि “ब्लैकआउट के दौरान हिंसक लामबंदी और तीव्र होती प्रतीत होती है.” इसलिए, यह सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है कि ऐसे ब्लैकआउट किसकी रक्षा करते हैं? उनकी संदिग्ध उपयोगिता के बावजूद, वैधता नही है.अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पारदर्शिता के उपाय इंटरनेट निलंबन आदेशों में पूरे नहीं किए गए. आईटी की संसदीय स्थायी समिति ने दर्ज किया कि सरकार ने जनवरी 2012 और मार्च 2021 के बीच भारत में कुल 518 बार इंटरनेट शटडाउन के आदेश दिए हैं. यह दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट ब्लॉकिंग है. हालाँकि, इस दावे को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय दोनों ही राज्यों द्वारा इंटरनेट बंद करने के आदेशों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं. क्या यह इतना शर्मनाक है कि इसे आधिकारिक रूप से गिना ही नहीं जाता है?
ऑनलाइन सेंसरशिप का दूसरा रूप है वेब सामग्री को अवरुद्ध करना है. जिससे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अनुलब्ध हो जाता है. हालाँकि, ये निर्देश अक्सर गुप्त रूप से दिए जाते हैं और सामग्री के अलग-अलग टुकड़ों के बजाय पूरे खाते को ब्लॉक कर दिया जाता है. यह किसी भी प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. ट्विटर का ही उदाहरण लें, 2014 में सरकार ने केवल 8 यूं आर एल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जब कि 2020 और 2021 में क्रमशः 2731 और 2851 खातों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. इन अवरोधक नियमों को पहले दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और अब ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं. पुलिस भारत के संविधान के हवाले से अपनी शक्तियो का प्रयोग करके वेबसाइट ब्लॉकिंग आमतौर पर प्रयोग में लाती है. उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे कानूनों के तहत नोटिस भेजे हैं, जिसके कारण डोमेन रजिस्ट्रारों को युवा पर्यावरण प्रचारकों की वेबसाइटों को ब्लॉक करना पड़ा. इनमें से कई किशोरों का अपराध केवल यह था कि उन्होंने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मानदंडों को कमजोर करने के खिलाफ पर्यावरण और वन मंत्रालय को लिखे ईमेल उपलब्ध कराना था. IFF में जब वकीलों अपील की तो इन नोटिसों को गलत माना गया और UAPA के संदर्भों को टाइपिंग की गलती बताई गयी.
क्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से पहले रुकना और सोचना संभव है?
तीसरा शायद ऑनलाइन सेंसरशिप का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण रूप है. इसे सीधे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब द्वारा लागू किया जाता है. जब वे अपने व्यवसाय और प्लेटफ़ॉर्म नीतियों में बैकएंड विकल्पों की भूलभुलैया के आधार पर उपयोगकर्ताओं को वांछित सामग्री के लिए अनुमति देते हैं, या प्रतिबंधित करते हैं, तो वे यह निर्धारित कर लेते हैं कि हम क्या देखते हैं, सोचते हैं और कैसी प्रतिक्रिया करते हैं. यह प्लेटफॉर्म सुविधाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो हमारे डिजिटल वातावरण की वास्तुकला प्रदान करता है. एक बार जब हमारी बातचीत कृत्रिम बुद्धि (ए आई)के माध्यम से संसाधित होती है जिसमे एनएलपी (प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण) मॉडल जैसी तकनीकों का उपयोग होता है, तब सामग्री मॉडरेशन का कार्य संचालन होने लगता है. हालांकि, मेरा मानना है कि मानव विवेक और समीक्षा के जरिए निर्णय लेने की काबिलियत अधिक महत्वपूर्ण है.
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सामग्री मॉडरेशन को वांछनीय होने का तर्क दिया जा सकता है क्योंकि यह हमारी रूचि के अनुरूप सामग्री दिखाकर हमारे मीडिया जुड़ाव में सुधार करता है. बाल यौन शोषण, नस्लीय और धार्मिक खतरों जैसे निषिद्ध सामाग्री को रोकता है. लेकिन यह सामग्री मॉडरेशन और नीति टीमों के व्यापक विवेक के लिए एक अपूर्ण प्रणाली है. ऐसे समाज में जहां कानून का शासन कमजोर है और जो साम्प्रदायिक तनावों से भरे हुए हैं, उसमें लिए गए निर्णय बाहरी प्रभावों से संचालित हो सकते हें. उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किये गए फेसबुक के आंतरिक पत्राचार के खुलासों के अनुसार, फेसबुक की भारत नीति टीम ने नफरती और भड़काऊ भाषणों के मामलों में अपनी सामग्री मॉडरेशन नीतियों को अमल में लाने पर रोक लगाया और इसका कारण अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और व्यावसायिक हितों के प्रभावित होने को बताया.यह अकारण नहीं है कि दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में फेसबुक की भूमिका की जांच शांति और सद्भाव समिति के जरिए करायी. इसके सम्मन को फेसबुक के मुख्य कार्यकारी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी. न्यायलय ने समिति सम्मन भेजने की शक्ति को बरकरार रखा. हालाँकि, बड़े विधायी ड्रामे के बाद भी इस मामले में बहुत कम हासिल किया गया है, जब कि इसकी कार्यवाही को YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया था. अंततः फेसबुक के प्रतिनिधि जब उपस्थित हुए तो भी उन्होंने टालमटोल ही किया. यह समिति अब 2021 से निष्क्रिय है. आज कल इसके अध्यक्ष एक संसद सदस्य हैं. इसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है. वास्तविक पारदर्शिता या उत्तरदायित्व के मामले में भी कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है. उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण दिल्ली विधानसभा की शक्तियां सीमित हैं. हमने प्रेस रिपोर्टों और लाइव स्ट्रीम में राजनीतिक प्रदर्शन और सार्वजनिक जागरूकता के कुछ स्तर जरूर देखे हैं.
यह विश्व स्तर पर माना जता है कि नागरिक विभाजन को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भूमिका होती है. यह भी है कि यह हिंसा से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने में स्वयंसेवी समूहों के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है. मुझे याद है, एक देर रात ट्विटर से एक युवा आयोजक के आह्वाहन पर मैं उसी समय आईटीओ के पास एक अस्थायी राहत केंद्र पर जाने वाले वकीलों के एक समूह में शामिल हो गया. वहां, हमने कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों में भोजन और चिकित्सा सामाग्री के वितरणकार्य का समन्वयकरण किया. यह हमारी आशा थी कि हमारी कारों पर वकीलों के पार्किंग स्टिकर लगे होने की वजह से, हमें इन इलाकों में या कम से कम स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक इस सामाग्री को पहुंचाने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा. मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया को बदनाम करने के जाल में फंसना आसान है, लेकिन जैसा कि फेसबुक व्हिसल-ब्लोअर फ्रांसिस हौगेन ने हमें याद दिलाया है, “एक सुरक्षित, अधिक सुखद सोशल मीडिया संभव है”. मानव समाज की उन्नति भ्रातृत्व और दया पर आधारित है. मौजूदाहाल में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए प्रोत्साहन सत्ता और लाभ के आसपास केंद्रित हैं. इसके बावजूद, मैंने 2020 में पहली बार देखा कि कैसे स्वयंसेवकों का एक छोटा सा समूह अपने साथी नागरिकों की भलाई के लिए सोशल मीडिया की शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम था, और हिंसा के पीड़ितों के लिए धन जुटा रहा था. दुर्भाग्य से, ये प्रयास भी सांप्रदायिकता की विभाजनकारी ताकतों से अछूते नहीं रह सके थे, धन संग्रह के प्रयासों को धार्मिक रेखा से विभाजित किया गया.
जन जागरूकता मुझे चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर ले जाती है जो सूचनाओं की बाढ़ ला कर व्याकुलता और विभाजन पैदा कर सकता है. जैसा कि ज़ेनेप तुफेकी कहते हैं, “इक्कीसवीं सदी में और नेटवर्क वाले सार्वजनिक क्षेत्र में, यह ज्यादा उपयोगी है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर उपलब्ध संसाधनों की तरफ ध्यान देने के बारे में सोचना अधिक उपयोगी है. और सेंसरशिप को सूचना का बाहर न निकलने देने के सक्रिय प्रयास के रूप तक सीमित नहीं करना चाहिए. कुछ प्लेटफ़ॉर्म सुविधाएओं द्वारा जैसे कि एक स्वचालित समाचार फ़ीड या विशेष रूप से ट्विटर ट्रेंड में उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर हैशटैग दिखाकर सार्वजनिक संवाद में हेरफेर किया जा सकता है. दंगे की स्थिति में हिंसा का आह्वान करने वाले और मीडिया उन्माद को बढ़ाने वाले ट्रेंडिंग विषय स्वचालित और मानवीय हस्तक्षेपों द्वारा मिल कर तैयार किये जाते है. इसके लिए फंड अक्सर राजनीतिक दलों और उनके सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिनका मकसद सामजिक ध्रुवीकरण करना होता है. इन विषयों के कुछ ट्वीट ऑनलाइन सहयोग टूल जैसे कि गूगल डॉक्स पर चिपकाए जाते हैं, फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बनाए गए समूहों को टेम्प्लेट के रूप में भेज दिए जाते हैं.फिर संदेशों की एक बाढ़ हमेशा हमारे स्मार्टफ़ोन में प्रवेश करती है और फिर निरंतर पिंग के माध्यम से यह हमें एक सांप्रदायिक माहौल में धकेल देती है. फिर बाक़ी लोगों की तरह निष्क्रिय प्रतिभागियों को, जो खुद को गैर राजनीतिक नागरिक कहते हैं उनके पास भी रुक कर विचार करने के लिए बहुत कम होता है. जैसा हैन्ना अर्देंट ने कहा है कि “कोई भी अथक गतिविधि जिम्मेदारी को भाप की तरह उड़ा देती है. एक अंग्रेजी मुहावरा है, “स्टॉप एंड थिंक.” कोई भी ब्यक्ति तब तक नहीं सोच सकता जब तक कि वे रुके नहीं…. और किसी ब्यक्ति में जिम्मेदारी केवल तब विकसित हो सकती है जब वह सोच विचार करे- स्वयं पर नहीं, बल्कि इस पर कि वह कर क्या रहा है.” सामाग्री की यह अथक बाढ़, जहां सामग्री की प्रकृति और निर्माण के पैमाने दोनों को सत्ता के ठेकेदारों, कानूनी विकारों, निजी लाभ और तकनीकी उपायों के संरचना का समर्थन हो तो वे स्थूल सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा देते हैं जो सामाजिक आक्रामकता की वकालत करता है, जैसा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तथ्यान्वेषी रिपोर्ट में नोट किया गया था कि “कई अपराधियों ने सोशल मीडिया पर हमलों को लाइव-स्ट्रीम किया, और हमले के उन वीडियो को अपलोड किया जिनमे वे खुद हिंसा कर रहे थे.” वे यह सब खुले आम और गर्व के साथ कर रहे थे.
मेरे लिए पांचवा मुख्य मार्ग है कि किस तरह नागरिक और आपराधिक कानूनों के डर के जरिए ऑनलाइन सूचना पारिस्थितिकी को क्यूरेट किया जाता है. यह विशेष रूप से उन लोगों को संबोधित है जो मानते हैं कि सोशल मीडिया के नुकसान की समस्या को लोगों पर और यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कठोर कानूनों और दंड के कानूनी प्रावधानों द्वारा हल किया जा सकता है. बस हमारे मौजूदा अनुभव को देखें. आज कल शिकायतें और मुकद्दमें निजी व्यक्तियों या अर्ध-सार्वजनिक सख्शियतों के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं, जो नोड की तरह या पुलिस विभागों की तरह कार्य करते हैं. ऐसे मामलों से अलोच्नामक रिपोर्टों के दमन को रोका जा सकता है. राजद्रोह, अश्लीलता के क़ानून और नफरती भाषणों सम्बंधित कानूनी प्रावधान के चलते पुलिस विभागों को सेंसरशिप की मांग करने और गिरफ्तारी को अमल में लाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं. आज कल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय पत्रकारों पर दिल्ली के धुंध की तरह एक बड़ी छाया मंडराती रहती है. उन्हें ऑनलाइन ट्रोल और यहां तक कि निजी व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो या न हो, अक्सर पुलिस विभागों के सोशल मीडिया हैंडल पर टैग किया जाता है. डिजिटल इंडिया में सेंसरशिप बंटी हुई है और हर किसी को आहत महसूस करने का पूरा अधिकार है. इसलिए, इंटरनेट भाषण और सेंसरशिप तंत्र, न केवल प्राकृतिक न्याय, या जनता के जानने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक अशांति में राज्य की जवाबदेही तै करने, हिंसा के दस्तावेज़ीकरण करने और राहत कार्यों के समन्वय में अड़चन पैदा करता है.
मीडिया के अन्य रूपों को एकीकृत करने के लिए इंटरनेट भी एक बोर्ग जैसा माध्यम है. उदाहरण के लिए, व्यापक मीडिया पारिस्थितिकी में सामाजिक विभाजनों को बढ़ाने और गहरा करने के लिए प्रोपेगैंडा की झलकियां अक्सर समाचार के रूप में सामने आती हैं. यहाँ समाचार एंकर रंगमंच के अभिनेताओं के समान अधिक दिखते हैं. संगीतमय मीम्स के साथ मिश्रित हो कर उनके समाचारों की कतरनें सोशल मीडिया पर एक बाढ़ की तरह छा जाती हैं. और उनके शो व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर आदान-प्रदान की जाने वाली सहज निजी बातचीत को गलत तरीके से एक बहस के रूप में पेश कर देते हैं.जब कोई पत्रकारिता की नैतिकता का सवाल सामने लाता है, तो वे उसके साथ संदेशवाहक को ही गोली मारने जैसा बर्ताव करते नज़र आते हैं. हालांकि, अब संदेशवाहक सन्देश ले जाने वाला कबूतर नहीं बल्कि एक गिद्ध है. इसी तरह हमारे मीडिया पारिस्थितिकी का एक चक्र पूरा होता है. और इस तरह के कई चक्र अलग-अलग रूप मौजूद हैं और वे हमारे स्मार्टफोन में लगातार बफर होते रहते हैं.
( यह शोध पत्र पूरा इस वेबसाईट पर मौजूद जन मीडिया 137 में पढ़ा जा सकता है)